मुद्रास्फीति क्या है?
5Paisa रिसर्च टीम
अंतिम अपडेट: 24 अप्रैल, 2023 04:47 PM IST
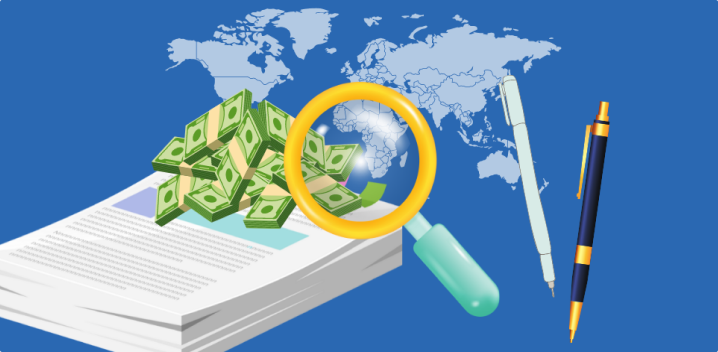
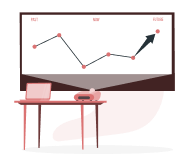
अपनी इन्वेस्टमेंट यात्रा शुरू करना चाहते हैं?
कंटेंट
- परिचय
- मुद्रास्फीति के मुख्य कारण क्या हैं?
- मुद्रास्फीति दर का अर्थ और सूत्र
- मुद्रास्फीति की गणना
- बढ़ती मुद्रास्फीति दर के प्रभाव
- मुद्रास्फीति के प्रकार
- आज मुद्रास्फीति और ऐतिहासिक मुद्रास्फीति के बीच क्या अंतर है?
- महंगाई कीमत को कैसे प्रभावित करती है?
- मुद्रास्फीति विस्फोट से कैसे अलग होती है?
- निष्कर्ष
परिचय
मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था में कुछ समय के दौरान सेवाओं और वस्तुओं की कीमतों के स्तर में क्रमिक वृद्धि को निर्दिष्ट करता है. इसका मतलब है कि पैसे की खरीद शक्ति सेवाओं और वस्तुओं की दर में वृद्धि के साथ कम हो जाती है. मुद्रास्फीति दर आमतौर पर एक वर्ष जैसे विशिष्ट समय में सामान्य कीमत के स्तर में प्रतिशत बदलाव को मापती है. तो, मुद्रास्फीति का क्या मतलब है? पैसे की आपूर्ति में वृद्धि, वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि या सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति में कमी जैसे विभिन्न कारक मुद्रास्फीति का कारण बन सकते हैं. उच्च मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, जैसे कम खरीद शक्ति, कम इन्वेस्टमेंट और बिज़नेस और उपभोक्ताओं के लिए अनिश्चितता में वृद्धि. मुद्रास्फीति के बारे में जानने के लिए पढ़ते रहें.
मुद्रास्फीति के मुख्य कारण क्या हैं?
जब अर्थव्यवस्था में पैसे सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, तो यह मुद्रास्फीति का कारण बनता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिक पैसा वही माल और सेवाओं का पीछा कर रहा है, जिससे कीमतें अधिक होती हैं. अगर किसी अर्थव्यवस्था में सेवाओं और वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, लेकिन आपूर्ति समान रहती है, तो कीमतों में वृद्धि होती है, जिससे मुद्रास्फीति हो सकती है.
जब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, तो बिज़नेस अपने लाभ मार्जिन को बनाए रखने के लिए अपनी कीमतें बढ़ा सकते हैं, जिससे मुद्रास्फीति हो सकती है. अगर सरकार टैक्स बढ़ाती है, तो यह माल और सेवाओं की लागत को बढ़ा सकती है, जिससे मुद्रास्फीति होती है.
अगर किसी करेंसी की वैल्यू अन्य करेंसी से संबंधित कम हो जाती है, तो इससे आयातित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ सकती है, जिससे मुद्रास्फीति होती है. प्राकृतिक आपदाएं या राजनीतिक अस्थिरता आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकती है, जिससे कमी, अधिक कीमतें और मुद्रास्फीति हो सकती हैं. नीचे आपको मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है इस बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी.
मुद्रास्फीति के प्राथमिक कारणों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है जैसे:
● मांग-पुल इफेक्ट
● बिल्ट-इन इन्फ्लेशन
● कॉस्ट-पुश इफेक्ट
● मांग-पुल प्रभाव
यह मुद्रास्फीति के प्रमुख कारणों में से एक है. यह अर्थव्यवस्था में सेवाओं और वस्तुओं की बढ़ती मांग के साथ होता है, लेकिन उनकी आपूर्ति मांग को पूरा नहीं कर पाती. इसके परिणामस्वरूप, कीमतें बढ़ने लगती हैं, जिससे मुद्रास्फीति होती है.
यह प्रभाव अक्सर आर्थिक विकास के दौरान देखा जाता है जब लोगों की अधिक डिस्पोजेबल आय होती है और अधिक खर्च करने के लिए तैयार होती है. यह मांग में वृद्धि जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कमी होती है, जो कीमतों को बढ़ा सकती है.
जब कीमतें बढ़ती हैं, तो बिज़नेस अपने लाभ मार्जिन को बनाए रखने के लिए अपनी कीमतें भी बढ़ा सकते हैं. यह एक साइकिल बना सकता है जहां कीमतें बढ़ती रहती हैं क्योंकि कंपनियां बढ़ी हुई मांग को पूरा करने की कोशिश करती हैं.
डिमांड-पुल इफेक्ट को सरकारी नीतियों द्वारा भी प्रभावित किया जा सकता है, जैसे स्टिमुलस पैकेज या टैक्स कट, जो उपभोक्ता खर्च को बढ़ा सकता है और सामान और सेवाओं की मांग को बढ़ा सकता है.
● लागत-पुश प्रभाव
मुद्रास्फीति का यह एक अन्य मुख्य कारण है. यह उत्पादन लागत में वृद्धि के साथ होता है, जिससे सेवाओं और वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि होती है. इसका कारण अक्सर मजदूरी में वृद्धि, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि या करों या विनियमों में वृद्धि जैसे कारकों के कारण होता है जो व्यवसाय करने की दर को बढ़ाता है.
बिज़नेस उच्च लागत का सामना करते समय उपभोक्ताओं को उच्च कीमतों के माध्यम से इन लागतों पर गुजर सकते हैं. यह एक साइकिल बना सकता है जहां उच्च कीमतें अधिक लागत तक पहुंचती हैं, और उच्च लागत से भी अधिक कीमतें होती हैं. प्राकृतिक आपदाओं, राजनीतिक अस्थिरता या वैश्विक आर्थिक स्थितियों जैसे बाहरी कारक भी लागत-पुश प्रभाव को प्रभावित कर सकते हैं.
● बिल्ट-इन इन्फ्लेशन
बिल्ट-इन मुद्रास्फीति पिछले मुद्रास्फीतिक दबावों और भविष्य में मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं के कारण होती है. यह तब होता है जब कर्मचारी और व्यवसाय जीवन की बढ़ती लागत के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए उच्च कीमतों और मजदूरी की अपनी अपेक्षाओं को समायोजित करते हैं.
बिल्ट-इन इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना कठिन है क्योंकि यह वास्तविक आर्थिक स्थितियों की बजाय भविष्य की अपेक्षाओं और धारणाओं पर आधारित है. हालांकि, सेंट्रल बैंक ब्याज़ दरों और मनी सप्लाई मैनेजमेंट जैसे मौद्रिक पॉलिसी टूल के माध्यम से मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को कम और स्थिर रखकर बिल्ट-इन मुद्रास्फीति को मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं. मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को कम रखकर, कामगारों और व्यवसायों को उच्च मजदूरी और कीमतों की मांग करने की संभावना कम हो सकती है, जो मुद्रास्फीतिक दबावों को कम करने में मदद कर सकती है.
मुद्रास्फीति दर का अर्थ और सूत्र
मुद्रास्फीति दर एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य और इसकी आर्थिक गतिविधि के स्तर को दर्शाता है. यह अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति क्या है यह बताता है. आमतौर पर स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लक्षण के रूप में कम और स्थिर मुद्रास्फीति दर देखी जाती है, जबकि उच्च या तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण चिंता हो सकती है क्योंकि इससे खरीद की क्षमता कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, और बिज़नेस और उपभोक्ताओं के लिए अनिश्चितता बढ़ जाती है.
केंद्रीय बैंक और सरकारें मुद्रास्फीति दर की निगरानी करती हैं और इसे प्रबंधित करने और कीमत की स्थिरता बनाए रखने के लिए विभिन्न आर्थिक और राजकोषीय नीतियों का उपयोग करती हैं.
फॉर्मूला:
इन्फ्लेशन रेट की गणना करने का यह फॉर्मूला है:
मुद्रास्फीति दर = (वर्तमान अवधि में प्राइस इंडेक्स - पिछली अवधि में प्राइस इंडेक्स) / पिछली अवधि में प्राइस इंडेक्स) x 100
इस फॉर्मूला में, प्राइस इंडेक्स आर्थिक सामान और सेवाओं की टोकरी की औसत कीमत को मापता है. यह आमतौर पर एक बेस वर्ष से संबंधित होता है, जहां बेस वर्ष के लिए प्राइस इंडेक्स 100 पर सेट किया जाता है.
मुद्रास्फीति की गणना
महंगाई की गणना करने के लिए, आपको इन चरणों का पालन करना होगा:
● माल और सेवाओं का एक बास्केट चुनें: मुद्रास्फीति की गणना करने का पहला चरण यह है कि अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं के आम खर्च पैटर्न का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तुओं और सेवाओं का बास्केट चुनें. वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधि होनी चाहिए, लोग खाद्य, आवास, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे खरीदते हैं.
● कीमतों पर डेटा इकट्ठा करें: अगला चरण बास्केट में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर डेटा इकट्ठा करना है. इस डेटा को सुपरमार्केट, हाउसिंग मार्केट या ऑनलाइन रिटेलर जैसे विभिन्न मार्केट में कीमतों का सर्वेक्षण करके प्राप्त किया जा सकता है. आपको मासिक या वार्षिक जैसे विभिन्न समय में वस्तुओं और सेवाओं की एक ही बास्केट कीमतों पर डेटा एकत्र करना होगा.
● प्राइस इंडेक्स की गणना करें: प्राइस डेटा एकत्र करने के बाद, आपको प्रत्येक अवधि के लिए प्राइस इंडेक्स की गणना करनी होगी. प्राइस इंडेक्स बास्केट में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का एक वेटेड औसत है, जहां वजन उपभोक्ताओं के कुल खर्च में प्रत्येक आइटम के शेयर हैं.
● इन्फ्लेशन रेट की गणना करें: अंत में, आप ऊपर दिए गए फॉर्मूला का उपयोग करके इन्फ्लेशन रेट की गणना कर सकते हैं.
बढ़ती मुद्रास्फीति दर के प्रभाव
बढ़ती मुद्रास्फीति दर में अर्थव्यवस्था और इसके लोगों पर मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रभाव हो सकते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:
● कम खरीद शक्ति: कीमतें बढ़ने के साथ, लोगों के पैसे की खरीद की शक्ति कम हो जाती है. इसका मतलब यह है कि लोग उसी राशि के साथ कम माल और सेवाएं खरीद सकते हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में गिरावट आती है.
● उच्च ब्याज़ दर: मुद्रास्फीति से निपटने के लिए, केंद्रीय बैंक परिसंचरण में पैसे की राशि को कम करने और धीमी गति से खर्च करने के लिए ब्याज़ दरें बढ़ा सकते हैं. इससे उधार लेना महंगा होता है, जिससे आर्थिक गतिविधि में मंदी आ जाती है.
● कम इन्वेस्टमेंट: उच्च मुद्रास्फीति दर का अर्थ अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता पैदा कर सकता है, जिससे भविष्य की योजना बनाना कठिन हो जाता है. इससे कम निवेश होता है, जो आर्थिक विकास को धीमा कर सकता है.
मुद्रास्फीति के प्रकार
कई प्रकार के मुद्रास्फीतियां हैं, जिनमें शामिल हैं:
1. मांग-पुल महंगाई: यह मुख्य रूप से होता है अगर आपूर्ति से संबंधित अर्थव्यवस्था में सेवाओं और वस्तुओं की अत्यधिक मांग होती है. जब मांग अधिक हो, तो उत्पादक कीमतों को बढ़ा सकते हैं, जिससे सामान्य कीमत स्तर बढ़ सकता है. यह आमतौर पर आर्थिक विकास से जुड़ा होता है और इसे कम बेरोजगारी दरों, बढ़े हुए सरकारी खर्च और आर्थिक नीति से चलाया जा सकता है.
2. लागत-पुश महंगाई: यह उत्पादन लागत में वृद्धि के साथ होता है जिससे सामान्य कीमत के स्तर में वृद्धि होती है. बढ़ती मजदूरी, उच्च इनपुट लागत, या सप्लाई चेन में बाधाएं इसका कारण बन सकती हैं. लागत-पुश मुद्रास्फीति से आउटपुट और रोजगार कम हो जाता है क्योंकि फर्म उच्च लागत को पूरा करने के लिए उत्पादन को कम करते हैं.
3. हाइपरिन्फ्लेशन: यह तब होता है जब मुद्रास्फीति दरें अत्यधिक उच्च स्तर तक बढ़ती हैं, आमतौर पर प्रति माह 50% से अधिक होती हैं. अधिक मुद्रास्फीति अक्सर आर्थिक संकट से जुड़ी होती है, जैसे युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता, और मुद्रा में लोगों का विश्वास खो देने के कारण आर्थिक प्रणाली के खराब हो जाती है.
4. रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन: यह तब होता है जब सरकार महंगाई को कृत्रिम रूप से दबाने के लिए पैसे की सप्लाई को नियंत्रित करती है या मूल्य निर्धारित करती है. हालांकि यह अस्थायी रूप से महंगाई दरों को कम कर सकता है, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था में विकृतियां भी हो सकती हैं, जैसे कि माल और सेवाओं की कमी और इन्वेस्टमेंट में कमी. दबाए गए मुद्रास्फीति से भविष्य में अधिक मुद्रास्फीति दरें भी हो सकती हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति के मुख्य कारणों को संबोधित नहीं किया जाता है.
5. ओपन इन्फ्लेशन: ओपन इन्फ्लेशन उस स्थिति को दर्शाता है जब ओपन मार्केट में कीमत बढ़ जाती है. इस प्रकार के मार्केट में, शासित या संबंधित अधिकारी मार्केट की कीमतों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं. खुले बाजार उत्पादन कारकों, कीमतों, निर्यात या आयात, उपभोग आदि पर नियंत्रण के बिना मुफ्त बाजार में कार्य करते हैं.
6. अर्ध-महंगाई: ऐसी स्थिति में, कीमतें धीरे-धीरे बढ़ सकती हैं, लेकिन धीरे-धीरे बढ़ सकती हैं, और बढ़ने की दर महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवधान या तुरंत पॉलिसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है. हालांकि, अर्ध-मुद्रास्फीति की अवधि में भी, खरीदने की क्षमता में कमी और आर्थिक वृद्धि और स्थिरता पर प्रभाव समय के साथ अभी भी महसूस किया जा सकता है.
आज मुद्रास्फीति और ऐतिहासिक मुद्रास्फीति के बीच क्या अंतर है?
मुद्रास्फीति आज कई तरीकों से ऐतिहासिक मुद्रास्फीति से भिन्न है:
● तीव्रता: आज मुद्रास्फीति आमतौर पर ऐतिहासिक स्तरों से कम होती है. उदाहरण के लिए, 1970 के दशक में, कई देशों में मुद्रास्फीति दरें दोहरे अंकों तक पहुंच गई हैं, जबकि आज, मुद्रास्फीति दरें आमतौर पर 5% से कम होती हैं.
● कारण: मुद्रास्फीति के कारण समय के साथ बदल गए हैं. भूतकाल में, महंगाई को अक्सर आपूर्ति-साइड शॉक से चलाया जाता था, जैसे तेल की कीमतों या भोजन की कीमतों में वृद्धि. आज, मुद्रास्फीति अक्सर मांग-साइड कारकों द्वारा चलाई जाती है, जैसे कि कम बेरोजगारी दरें और आर्थिक नीति में कमी.
● सेंट्रल बैंक की स्वतंत्रता: कई देशों में, सेंट्रल बैंकों ने हाल के दशकों में राजनीतिक प्रभाव से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त की है. इससे उन्हें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अधिक प्रभावी आर्थिक नीतियों को लागू करने की अनुमति मिली है.
● वैश्वीकरण: वैश्वीकरण के माध्यम से अर्थव्यवस्थाओं के बढ़े हुए एकीकरण से सामान और सेवाओं के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा और कम कीमतें हुई हैं. इससे कई देशों में मुद्रास्फीति दरों की जांच करने में मदद मिली है.
● टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट: टेक्नोलॉजी में एडवांस से उत्पादकता और कार्यक्षमता बढ़ गई है, जिससे उत्पादन लागत कम हो जाती है और महंगाई दरों को कम रखने में मदद मिली है.
● जनसांख्यिकी: कई विकसित देशों में वृद्धावस्था की आबादी जैसे जनसांख्यिकी में परिवर्तन से मुद्रास्फीति की दरें कम हो गई हैं. पुरानी आबादी अधिक बचत करती है और कम खर्च करती है, जो मांग को कम कर सकती है और कीमतें नियत रख सकती हैं.
कुल मिलाकर, महंगाई कई पॉलिसी निर्माताओं के लिए चिंता रहती है, लेकिन आज महंगाई की प्रकृति और परिमाण ऐतिहासिक स्तरों से काफी अलग है.
महंगाई कीमत को कैसे प्रभावित करती है?
मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में कीमत पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है. जब मुद्रास्फीति के कारण सामान्य कीमत का स्तर बढ़ता है, तो यह उत्पादकों और उपभोक्ताओं को अलग-अलग प्रभावित करता है. मुद्रास्फीति की कीमतों को प्रभावित करने के कुछ तरीके यहां दिए गए हैं:
1. उत्पादन की लागत: जब मुद्रास्फीति होती है, तो माल और सेवाओं के उत्पादन की कीमत बढ़ जाती है. यह कच्चे माल की कीमतें, मजदूरी या परिवहन लागतों के कारण हो सकता है. इसके परिणामस्वरूप, उत्पादक अपने लाभ मार्जिन को बनाए रखने के लिए कीमतें बढ़ा सकते हैं.
2. उपभोक्ता की मांग: मुद्रास्फीति उपभोक्ता की मांग को भी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि बढ़ती कीमतें उपभोक्ताओं की खरीद शक्ति को कम कर सकती हैं. अगर कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, तो उपभोक्ता खर्च को कम कर सकते हैं, बिज़नेस सेल्स को कम कर सकते हैं. दूसरी ओर, अगर कीमतें धीरे-धीरे और धीरे धीरे बढ़ती हैं, तो उपभोक्ता उच्च कीमतों को समायोजित करने के लिए अपनी खर्च की आदतों को समायोजित कर सकते हैं.
3. प्रतिस्पर्धा: मुद्रास्फीति भी बिज़नेस के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकती है. इसके अलावा, अगर उनके प्रतिस्पर्धी कीमतें भी बढ़ा रहे हैं, तो कंपनियां कस्टमर को खोए बिना कीमतें बढ़ा सकती हैं. अन्य मामलों में, बिज़नेस को प्रतिस्पर्धी रहने के लिए उच्च लागत को अवशोषित करना पड़ सकता है.
4. आर्थिक नीति: केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक नीति को समायोजित कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, वे मांग को कम करने और मुद्रास्फीति को कम करने के लिए ब्याज़ दरों को बढ़ा सकते हैं. यह बिज़नेस के लिए पैसे उधार लेने के लिए अधिक महंगे बनाकर कीमतों को प्रभावित कर सकता है, जो इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन को कम कर सकता है.
मुद्रास्फीति विस्फोट से कैसे अलग होती है?
मुद्रास्फीति और विस्फोट के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं:
1. उधारकर्ताओं और लेंडर पर प्रभाव: मुद्रास्फीति उधारकर्ताओं को लाभ पहुंचाती है क्योंकि उनके क़र्ज़ की वास्तविक वैल्यू समय के साथ कम हो जाती है, जबकि लेंडर को उनकी एसेट की वास्तविक वैल्यू कम होती है. विस्फोट में, विपरीत सच है - उधारकर्ताओं को उनके ऋण का वास्तविक मूल्य बढ़ जाता है, जबकि लेंडर अपनी परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य बढ़ने के कारण लाभ प्रदान करते हैं.
2. आर्थिक विकास पर प्रभाव: मध्यम महंगाई उपभोक्ता खर्च और निवेश को प्रोत्साहित करके आर्थिक विकास को लाभ पहुंचा सकती है. हालांकि, उच्च मुद्रास्फीति से अनिश्चितता और अस्थिरता होती है, जो आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचाती है. महंगाई आर्थिक विकास को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे खर्च और निवेश कम हो सकता है.
3. कारण: मुद्रास्फीति आमतौर पर बढ़ती मांग, सप्लाई शॉक या मौद्रिक पॉलिसी खो जाने जैसे कारकों के कारण होती है. डिफ्लेशन कम मांग, सप्लाई ग्लट या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जैसे कारकों के कारण हो सकता है.
कुल मिलाकर, मुद्रास्फीति और विस्फोट किसी अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य स्तर में विपरीत गतिविधियां होती हैं, और वे विभिन्न आर्थिक अभिनेताओं और आर्थिक विकास पर मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रभाव डाल सकते हैं.
निष्कर्ष
अंत में, मुद्रास्फीति का अर्थ समय के साथ सेवाओं और वस्तुओं की कीमत में निर्धारित वृद्धि को निर्दिष्ट करता है. मांग-पुल, कॉस्ट-पुश और बिल्ट-इन इन्फ्लेशन सहित विभिन्न कारकों के कारण इसे होता है. मुद्रास्फीति के स्तर और दृढ़ता के आधार पर अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं.
जबकि मध्यम महंगाई बढ़ते उपभोक्ता खर्च और निवेश द्वारा आर्थिक वृद्धि को प्रेरित कर सकती है, उच्च या अप्रत्याशित महंगाई जिससे वित्तीय अस्थिरता और हानिकारक आर्थिक विकास हो सकती है.
सरकार और केंद्रीय बैंक महंगाई को प्रबंधित करने के लिए विभिन्न टूल का उपयोग करते हैं, जैसे ब्याज़ दरों को समायोजित करना और राजकोषीय नीति को निष्पादित करना. उपभोक्ताओं, व्यवसायों और नीति निर्माताओं के लिए मुद्रास्फीति को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कीमतों, मजदूरी, ब्याज़ दरों और आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है.
जेनेरिक के बारे में अधिक
- TTM (ट्रेलिंग ट्वेल्व महीने)
- UPI में वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA) क्या है?
- सर्वश्रेष्ठ स्विंग ट्रेडिंग रणनीतियां
- एफडी लैडरिंग क्या है?
- घर खरीदने के लिए क्रेडिट स्कोर की आवश्यकता क्या है?
- जॉब लॉस से कैसे निपट सकते हैं?
- क्या 750 अच्छा क्रेडिट स्कोर है?
- क्या 700 अच्छा क्रेडिट स्कोर है?
- इम्पल्स खरीदना क्या है?
- Fico स्कोर बनाम क्रेडिट स्कोर
- अपनी क्रेडिट रिपोर्ट से विलंब भुगतान कैसे हटाएं?
- अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट कैसे पढ़ें?
- क्या कार इंश्योरेंस का भुगतान क्रेडिट बनाता है?
- कैशबैक बनाम रिवॉर्ड पॉइंट
- टालने के लिए 5 सामान्य क्रेडिट कार्ड गलतियां
- मेरा क्रेडिट स्कोर क्यों गिरा?
- CIBIL रिपोर्ट कैसे पढ़ें
- क्रेडिट स्कोर में सुधार करने में कितना समय लगता है?
- CIBIL रिपोर्ट में पिछले देय दिन (DPD)
- CIBIL बनाम एक्सपीरियन बनाम इक्विफैक्स बनाम हाईमार्क क्रेडिट स्कोर
- सिबिल स्कोर के बारे में 11 सामान्य अफवाहें
- टैक्टिकल एसेट एलोकेशन
- प्रमाणित फाइनेंशियल सलाहकार क्या है?
- वेल्थ मैनेजमेंट क्या है?
- कैपिटल फंड
- आरक्षित निधि
- बाजार भावना
- एंडोमेंट फंड
- आकस्मिकता निधि
- कंपनियों का रजिस्ट्रार (आरओसी)
- इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो
- फ्लोटिंग रेट नोट
- आधार दर
- एसेट-बैक्ड सिक्योरिटीज़
- एसिड-टेस्ट रेशियो
- भाग लेने वाले प्राथमिकता शेयर
- खर्चों की ट्रैकिंग क्या है?
- क़र्ज़ समेकन क्या है?
- NRE और NRO के बीच अंतर
- ऋण समीक्षा
- पैसिव निवेश
- पेपरलेस लोन कैसे प्राप्त करें?
- CIBIL डिफॉल्टर लिस्ट कैसे चेक करें?
- क्रेडिट स्कोर बनाम सिबिल स्कोर
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)
- स्टेच्युटरी लिक्विडिटी रेशियो (SLR)
- कैश मैनेजमेंट बिल (CMB)
- सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट (SOFR)
- पर्सनल लोन बनाम बिज़नेस लोन
- व्यक्तिगत फाइनेंस
- क्रेडिट मार्केट क्या है?
- ट्रेलिंग स्टॉप लॉस
- सकल एनपीए बनाम नेट एनपीए
- बैंक दर बनाम रेपो दर
- ऑपरेटिंग मार्जिन
- गियरिंग रेशियो
- जी एसईसीएस - भारत में सरकारी प्रतिभूतियां
- प्रति व्यक्ति आय भारत
- टर्म डिपॉजिट क्या है
- रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो
- देनदारों का टर्नओवर अनुपात
- टेकओवर
- बैंकिंग में IMPS पूरा फॉर्म
- डिबेंचरों का रिडेम्पशन
- 72 का नियम
- संस्थागत निवेशक
- पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय
- निवल आय क्या है
- परिसंपत्तियां और देनदारियां
- सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)
- नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर
- मुद्रास्फीति सूचकांक
- बुक वैल्यू क्या है?
- उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति क्या हैं?
- फिक्स्ड डिपॉजिट के प्रकार
- निवल लाभ क्या है?
- नियो बैंकिंग क्या है?
- फाइनेंशियल शेनानिगन्स
- चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी
- बैंक अनुपालन क्या है?
- सकल मार्जिन क्या है?
- अंडरराइटर क्या है?
- मेच्योरिटी (वायटीएम) की उपज क्या है?
- मुद्रास्फीति क्या है?
- जोखिम के प्रकार
- सकल लाभ और निवल लाभ के बीच क्या अंतर है?
- कमर्शियल पेपर क्या है?
- एनआरई खाता
- एनआरओ खाता
- रिकरिंग डिपॉजिट (RD)
- उचित बाजार मूल्य क्या है?
- उचित मूल्य क्या है?
- एनआरआई क्या है?
- CIBIL स्कोर के बारे में बताया गया है
- निवल कार्यशील पूंजी
- ROI - इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न
- मुद्रास्फीति का कारण क्या है?
- कॉर्पोरेट क्रिया क्या है?
- SEBI क्या है?
- फंड फ्लो स्टेटमेंट
- इंटरेस्ट कवरेज रेशियो
- मूर्त आस्तियां बनाम. अमूर्त आस्तियां
- करंट लायबिलिटी
- वर्तमान अनुपात समझाया गया - उदाहरण, विश्लेषण और गणना
- प्रतिबंधित स्टॉक यूनिट (आरएसयू)
- लिक्विडिटी रेशियो
- ट्रेजरी बिल
- पूंजीगत व्यय
- नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए)
- UPI ID क्या है? अधिक पढ़ें
डिस्क्लेमर: सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट मार्केट जोखिमों के अधीन है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले सभी संबंधित डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें. विस्तृत डिस्क्लेमर के लिए कृपया यहां क्लिक करें.
मुफ्त डीमैट अकाउंट खोलें
5paisa कम्युनिटी का हिस्सा बनें - भारत का पहला लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मुद्रास्फीति की परिभाषा के अनुसार, मुद्रास्फीति मुख्य रूप से तब होती है जब कमोडिटी और सर्विसेज़ की कीमत में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है क्योंकि करेंसी की खरीद शक्ति में धीरे-धीरे नुकसान होता है.
मुद्रास्फीति के कई लाभ हैं, जैसे:
● उच्च लाभ
● अधिक रोजगार और बेहतर आय
● बेहतर इन्वेस्टमेंट रिटर्न
● उधारकर्ताओं को लाभ
● उत्पादन में वृद्धि
मुद्रास्फीति की रोकथाम के कई तरीके हैं, जैसे:
● मौद्रिक पॉलिसी
● राजकोषीय पॉलिसी
● सप्लाई-साइड पॉलिसी
● वेतन और कीमत नियंत्रण
मुद्रास्फीति के मुख्य प्रकार हैं:
● मांग-पुल इन्फ्लेशन
● कॉस्ट-पुश इन्फ्लेशन
● हाइपरइन्फ्लेशन
● रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन
● मुद्रास्फीति खोलें
● सेमी-इन्फ्लेशन
मुद्रास्फीति को मापने का फॉर्मूला है:
मुद्रास्फीति दर = (वर्तमान अवधि में प्राइस इंडेक्स - पिछली अवधि में प्राइस इंडेक्स) / पिछली अवधि में प्राइस इंडेक्स) x 100
